History
लघु उत्तरीय प्रश्न
1.मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दें ।
साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य (चाणक्य) कृत अर्थशास्त्र विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस विष्णु पुराण बौद्ध एवु जैन धर्मग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है । विदेशी यात्रियों के विवरणों में यूनानी राजदूत, मेगास्थानीज की इण्डिका, मौर्यकालीन इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख एवं सिक्के मौर्यकालीन इतिहास को लिखने में अत्यधिक प्रमाणिक एवं मददगार साबित हुए हैं।
2.अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें ।
अपनी प्रजा के उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की सहिता प्रस्तुत की उसके अभिलेखों में 'धम्म' कहा गया है। अशोक अपने दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेख में धम्म क्या है का उत्तर स्वयं देता है। 'अपासिनवे बहू कयाने दाया दाने सचे सोचये चखु दाने पि में बहुविधे दिने दुपद
अर्थात्
• धम्म
1. अल्प पाप है
2. माता-पिता की सेवा करना,
3. दया है
4. दान
5. सत्यवादिता है
6. पवित्रता है
7. मृदुता है
अशोक यह भी बताता है कि धम्म पालन
1. प्राणियों की हत्या न करना,
2. निष्ठुरता
3. वृद्धों की सेवा करना,
4. गुरुजनों का सम्मान करना, के साथ अच्छा व्यवहार करना,
5. मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, ग्रामीणों एवं दासों
6. अल्प व्यय एवं अल्प संचय अशोक ने
अशोक का वारणा पर आधारित है । धम्म सभी धर्मों का सार है यह सर्वधर्म समभाव एवं वसुधैव कुटम्बकम की
3. चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें ।
चन्द्रगुप्त द्वितीय न केवल एक महान विजेता बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। गुप्त प्रशासन का निर्माण उसी ने किया । उसका 40 वर्षों का दीर्घकालीन शासन शांति, सुव्यवस्था और संवृद्धि का काल था ।
चन्द्रगुप्त द्वितीय की प्रमुख उपलब्धियाँ
(i) बंगाल के युद्ध क्षेत्र में उसने शत्रुओं के एक संघ को पराजित किया था ।
(ii) सिंधु के सातों मुखों को पार कर उसने बाहिलको को जीता था ।
(iii) दक्षिण भारत में उसकी ख्याति फैली हुई थी ।
(iv) वह भगवान विष्णु का परमभक्त था ।
4.गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें ।
गौतम बुद्ध का जन्म 563 ई० पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल के क्षेत्रिय वंशीय राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। उनके बचपन में ही उनकी माता महामाया का देहान्त हो जाने कारण मौसी गौतमी ने उनका पालन पोषण किया । 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक सुंदरी से उसका विवाह हुआ तथा 28वें वर्ष उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। उन्होंने सांसारिक दुखों से द्रवित होकर 29वें वर्ष गृह त्याग दिया । 35 वर्ष की आयु ज्ञान की प्राप्ति हुये । 483 ई० पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका निधन हुआ गया (बिहार) में उर्वला नामक स्थान पर
बौद्ध धर्म के उपदेश :
गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रर्वतक थे। उन्होंने सांसारिक दुखों के चार कारण बताए :
1. जीवन दुखमय है
2. तृष्णा, मोह, लालसा, दुख के कारण हैं,
3. इन कारणों को दुखों से छुटकारा पाया करके जा सकता है और
4. उसके लिए सत्य मार्ग का ज्ञान आवश्यक ।
5. बलबन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें ।
बुद्ध ने दुःख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का प्रावधान किया सम्यक् भाषण 2. सम्यक् कर्म 3. सम्यक् प्रयत्न, 4. सम्यक् भाव 5. सम्यक् ध्यान 6. सम्यक् संकल्प 7. सम्यक् दृष्टि 8. सम्यक् निर्वाह । बलबन इल्तुतमिश के चहलगानी दल का सदस्य था । बलबन ने राजत्व का एक नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया । बलबन ने एक केन्द्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की एवं गुप्तचर विभाग का भी संगठन किया । उसने पहली बार मंगोलों से बचाव के लिए सीमान्त क्षेत्रों में दुर्ग का निर्माण करवाया और वहाँ योग्य सेना भूदयक्षों को नियुक्त किया। बलबन कुरान के नियमों को शासन का आधार मानता था । बलबन ने ईश्वर, शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को राज्य का आधार बनाने का प्रयत्न किया ।
6.मनसबदारी व्यवस्थ की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें ।
अकबर ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनसबदारी व्यवस्था का प्रवर्तन किया। यह दसमलव प्रणाली पर आधारित था। मनसबदार को दो पद जात एवं सवार प्रदान किए जाते थे। ब्लाकमैन के अनुसार, एक मनसबदार को अपने जितने सैनिक रखने पड़ते थे वह जात का सूचक था । वह जितने घुड़सवार रखता था वह सवार का सूचक था ।
40 से 500 तक का मनसबदार 'मनसबदार' कहलाता था। 500 से 2500 का मनसबदार अमीर कहलाता था । 2500 से अधिक का मनसबदार अमीर ए उम्दा कहलाता था ।
मनसबदारों में वेतन में नकद रकम मिलता था। कभी-कभी वेतन में जागीर भी दी जाती थी इस प्रकार मनसबदारी व्यवस्था मुगल सेना का प्रमुख आधार बन गयी। उसने मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं सुव्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनायी ।
7.कबर की धार्मिक नीति की समीक्षा करें ।
1563 ई० में अकबर ने तीर्थ यात्री कर बंद कर दिया । अकबर ने सभी धर्मों की अच्छायियों का सार प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसी कोशिश के तहत 1581 ई० में उसने दीन-ए-इलाही का प्रवर्तन किया। उस धर्म के द्वारा अकबर ने हिंदू व मुस्लिम धर्म को मिलाकर साम्राज्य में राजनीतिक एकता कायम करने की कोशिश की। 1564 ई० में अकबर ने जजिया कर बंद कर दिया। यह समस्त भारत में गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था ।
अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनायी । 1563 ई० में अकबर ने तीर्थ यात्री कर बंद कर दिया । अकबर ने सभी धर्मों की अच्छायियों का सार प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसी कोशिश के तहत 1581 ई० में उसने दीन-ए-इलाही का प्रवर्तन किया । उस धर्म के द्वारा अकबर ने हिंदू व मिलाकर साम्राज्य में राजनीतिक एकता कायम करने की कोशिश की । 1564 ई० जजिया कर बंद कर दिया। यह समस्त भारत में गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता मुस्लिम में धर्म को अकबर ने था ।
8. स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गाँधी की भूमिका पर प्रकाश डालिए ।
स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गाँधी की अग्रणी भूमिका है। 1917 ई० में चंपारण के कृषकों को उन्होंने नील उत्पादक गोरों के अत्याचारों से मुक्ति दिलायी । 1917 ई० में ही अहमदाबाद के मिल-मालिकों तथा श्रमिकों के बीच उत्पन्न प्लेग बोनस के विवाद को हल करने में उन्होंने अपना योगदान दिया । 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया । 1930 ई० में गाँधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दाण्डी यात्रा की और नमक कानून को भंग किया। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और अन्ततः उनके महत्वपूर्ण योगदान के परिणामस्वरूप 15 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ ।
9. भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें ।
महात्मा गाँधी ने 1942 ई० में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध महात्मा गाँधी का यह अंतिम आंदोलन था। जिसमें उन्होंने 'करो या मरो' का नारा दिया। भारत का विशाल जन सैलाव महात्मा गाँधी के नेतृत्व में साथ खड़ा हुआ । यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की चरम सीमा था । उससे ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीयों का क्रोध व्यक्त हुआ। इतने विशाल जन आंदोलन से ब्रिटिश सरकार घबरा गयी और अन्ततः उन्होंने भारत छोड़ने का निश्चय कर लिया और अन्ततः 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ ।
10. कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका का परीक्षण करें ।
उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम अथवा बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक नए एवं
तरूण दल का उदय हुआ जो पुराने नेताओं के आदर्श तथा ढंगों का प्रखर आलोचक था । उनका ध्येय था कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज होना चाहिए । वे कांग्रेस के उदारवादी नीतियों का विरोध करते थे । 1905 से 1919 का काल भारतीय इतिहास में उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है । उस युग के नेताओं में बालगंगाधर तिलक, विपिन चन्द्रपाल, लाला लाजपत राय आदि प्रमुख थे । उग्रवादियों ने विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल अंगीकार करने पर बल दिया । दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्राचीन भारतीय
11.इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें ।
(i) प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं :
(i) पुरातात्विक स्रोत
(ii) साहित्यिक स्रोत
(iii) विदेशी विवरण
पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक और भवन मूर्तियाँ आदि प्रमुख हैं । अभिलेख : पुरातात्विक स्रोतों के अन्तर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख अभिलेख अशोक के हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्रह्मी लिपि में है। अन्य अभिलेखों में । सबसे प्राचीन खारवेल का हाथिगुम्फा अभिलेख, नासिक अभिलेख, जूनागढ़ शिलालेख आदि । अभिलेखों के अध्ययन से तत्कालीन शासकों के राजनीतिक विस्तार के अध्ययन पर प्रकाश पड़ता सिक्के: प्राचीन भारत के अध्ययन के है । पुरातात्विक ' लिखा है । स्रोतों में सिक्कों का स्थान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । इन सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त संभवतः व्यापारियों श्रेणियों, नगरनिगमों ने चालू किया था। इनसे इतिहासकारों को विशेष सहायता नहीं मिली है। मुद्रा के अध्ययन से देश की आर्थिक स्थिति की विशेष जानकारी प्राप्त होती है उसके अतिरिक्त सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक महत्व की चीजों की भी जानकारी उससे प्राप्त होती है । समुद्रगुप्त के सिक्कों पर ग्रूप बना है और 'अश्वमेघ पराक्रम स्मारक और भवन प्राचीनकाल के महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है। उत्तर भारत के मंदिरों की शैली नागर शैली तथा दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है । बनायी • मूर्तियाँ: उसी प्रकार प्राचीन काल में कुषाणों, गुप्त शाषकों, गुप्ततोत्तर शासकों ने जो मूर्तियाँ उनसे जनसाधारण की धार्मिक अवस्थाओं और मूर्तिकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है।
(ii) साहित्यिक स्रोत-साहित्य दो प्रकार का है : (i) धार्मिक साहित्य (ii) लौकिक साहित्य |
गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारतीय इतिहास के उस युग का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सभ्यताओं संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई तथा हिंदू संस्कृति अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुँच गयी । गुप्तकाल की चहुमुखी प्रगति को ध्यान में रखकर ही इतिहासकारों ने उस काल को स्वर्ण युग (Golden Age) की संज्ञा से अभिहित किया है ।
12. चन्द्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों की विवेचना करें ।
चन्द्रगुप्त मौर्य भारत में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चन्द्रगुप्त मौर्य भारत के उन महानतम सम्राटों में हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व तथा कृतियों से इतिहास के पृष्ठों में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न किया है। उसका उदय वस्तुतः इतिहास की एक रोमांचकारी घटना है। देश को मूकदूवी दासता से मुक्त करने तथा नन्दों के घृणित एवं अत्याचारपूर्ण शासन से जनता को त्राण दिलाने तथा देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में संगठित करने का श्रेय उसी सम्राट को प्राप्त है
चीन भारतीय इतिहास के उस युग का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सभ्यताओं संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई तथा हिंदू संस्कृति अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुँच गयी । गुप्तकाल की चहुमुखी प्रगति को ध्यान में रखकर ही इतिहासकारों ने उस काल को स्वर्ण युग (Golden Age) की संज्ञा से अभिहित किया है ।
निश्चिततः यह काल अपने प्रतापी राजाओं और अपनी सर्वोत्कृष्ठ संस्कृति के कारण भारतीय इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण के समान प्रकाशित है। मानव जीवन के सभी क्षेत्रों ने उस समय प्रफुल्लता एवं समृद्धि के दर्शन किये थे ।
निम्न विशेषताओं के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का 'स्वर्ण युग' माना जाता है :
(i) राजनीतिक एकता का काल
(ii) महान सम्राटों का काल
(iii) आर्थिक समृद्धि का काल
(iv) धार्मिक सहिष्णुता का काल
(v) श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का काल
(vi) साहित्य, विज्ञान एवं कला के चरमोत्कर्ष का काल
(vii) भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल ।
उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य गुप्त साम्राज्य को स्वर्णयुग माना जाता है। किन्तु कुछ आधुनिक युग के इतिहासकार जिसमें आर० एस० शर्मा रोमिला थापर आदि प्रमुख हैं। गुप्तकाल को स्वर्णयुग कहना उचित नहीं मानते हैं ।
13. कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करें ।
1205-06 ई० में मुहम्मद गोरी जब खोखरों को हराकर गजनी वापस लौट रहा था तो उसने औपचारिक रूप से ऐबक को अपने भारतीय ठिकानों का प्रतिनिधि नियुक्त किया । गोरी की अकास्मिक मृत्यु के कारण उत्तराधिकारी के संबंध में निर्णय नहीं हो पाया था । 1208 से 1210 तक वह स्वतंत्र भारतीय राज्य का औपचारिक अधिकार प्राप्त शासक था । वह एक कुशल सैनिक था । ऐबक की उपलब्धियाँ एक विजेता की थी किंतु वह अपने दिल और दिमाग की विशेषताओं के लिए समकालीन इतिहासकारों द्वारा सराहा भी गया है, न्यायप्रियता और सुरक्षा की भावना उसके राज्य की विशेषता थी । जनता को शांति और समृद्धि देना उसने अपना कर्त्तव्य समझा । युद्ध की स्थिति खत्म होने के बाद उसने जनता के हितों की रक्षा की और उनकी समृद्धि की ओर ध्यान दिया। उसकी उदारता के कारण उसे 'लाख बख्श' कहा गया । 1210 ई० में घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई और वह अपने कार्यों को अधूरा छोड़ गया। उसने कुतुबमीनार का कार्य आरंभ 1 * करवाया था ।
14. प्लासी युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें ।
औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य छिन्न-भिन्न होना आरंभ हो गया तथा साम्राज्य के कई भाग विभिन्न नवावों के अधीन स्वतंत्र हो गए। बंगाल में 1740 तक अलवर्दी खान ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। उसमें अनुपम कार्यक्षमता तथा असाधारण योग्यता थी । उसने अंग्रेजों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहारं बनाया लेकिन यह आज्ञा नहीं दी कि वे अपनी बस्तियों में किले वनवा सकें । वह 1556 तक शासन करता रहा।
अलवर्दीखान की मृत्यु के बाद उसका पोता सिराजुद्दौला बंगाल का नवाव बना । उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर उनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष शुरू हुआ । उस संघर्ष के बहुत से कारण थे। 'सप्तवर्षीय युद्ध' छिड़ने की आशंका से अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी बस्तियों में दुर्ग बनाने आरंभ कर दिए । चूंकि उन्होंने वह सब कुछ नबाव की अनुमति के बिना किया इसलिए नवाव ने उन्हें आज्ञा दी कि वे उन दुर्ग को गिरा दें। किंतु अंग्रेजों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। उसके साथ ही अंग्रेजों ने सिराजुदौला के प्रतिद्वन्द्वी शैकतजंग का पक्ष लिया। अंग्रेजों ने बंगाल के एक धनी व्यापारी को शरण दी तथा उसे नवाव के सुपुर्द करने से इन्कार कर दिया । नवाव ने यह भी आरोप लगाया कि जो व्यापारिक सुविधाएँ अंग्रेजों को सरकार की ओर से प्रदान की गई थी वे उनका अनुचित उपयोग कर रहे थे ।
परिणामस्वरूप सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार में अंग्रेजी कारखाने पर अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता के नगर पर भी अधिकार कर लिया । 146 व्यक्तियों को पकर लिया गया जिनमें से एक स्त्री भी थी । उन्हें रात्रि के समय एक बंद कमरे में रखा गया। गर्मी इतनी अधिक थी तथा स्थान इतना कम था कि उनमें से 123 व्यक्ति दम घुट जाने के कारण मर गए। उस दुर्घटना को ब्लैकहॉल के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकार उस घटना को कोरी कल्पना माना हैं। अंग्रेजों ने इस घटना को बहाना बनाकर नवाव के विरुद्ध षडयंत्र रचने लगा। नवाब के कोषाध्यक्ष रायदुर्लभ, नवाव के सेनापति मीरजाफर; बंगाल के सबसे सम्पन्न बैंकर जगत सेठ इन सबको नवाव के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भड़काया ।
1757 में क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना प्लासी के मैदान में सिराजुदौला को हराया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी ।
प्लासी के युद्ध का यह परिणाम हुआ कि मीर जाकर को बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया। उसने चौबीस परगने तथा एक करोड़ रुपए कंपनी को दिए । उसने कंपनी के अन्य अंग्रेज अफसर को भी उपहार दिए । एडमिरल वाटसन के शब्दों में "प्लासी का युद्ध कंपनी के लिए ही नहीं अपितु सामान्य रूप से ब्रिटिश जाति लिए असाधारण महत्व रखता था।"
15. असहयोग आंदोलन की प्रकृति एवं परिणामों का वर्णन करें ।
कांग्रेस ने महात्मा गाँधी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। यह सचमुच एक क्रांतिकारी कदम था । इस आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय था। यह देश का प्रथम जन आंदोलन था। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक उस आंदोलन का प्रसार था। पहली बार सभी धर्मों, जातियों के लोगों ने एक साथ आंदोलन में भाग लिया। स्त्रियों की भागेदारी उस आंदोलन की एक अन्य विशेषता है। सरकारी वस्तुओं का बहिष्कार करना शान का विषय बन गया था। जेल जाना आम बात हो गई थी। कांग्रेस की प्रवृति में भी बदलाव आया एवं संवैधानिक उपायों की प्रासंगिकता समाप्त हो गयी। जनता में संघर्ष करने का नया जोश पैदा हुआ। संपूर्ण देश में जनता ने बड़े ही उत्साह के साथ उसमें भाग लिया ।
आंदोलन के परिणाम :
इस आंदोलन के दूरगामी परिणाम सिद्ध हुए
(i) यह एक जन आंदोलन था। इसमें बड़े से बड़े और छोटे व्यक्ति ने भाग लिया ।
(ii) स्वदेशी आंदोलन विशेष रूप से खादी चरखे से आत्म विश्वास की भावना का विकास हुआ।
(iii) उस आंदोलन में सभी पक्षों पर जिनमें शिक्षा, आर्थिक व सामाजिक सभी पर समान जोर दिया गया था ।
(iv) ब्रिटिश सरकार का भय अब जनता के मन से निकल गया ।
(v) पहली बार महिलाओं ने जोरदार ढंग से राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी । जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में "गाँधीजी के असहयोग आंदोलन ने आत्मनिर्भरता तथा शक्ति संचय का पाठ पढ़ाया । सरकार भारतीयों के एच्छिक अथवा अनैच्छिक सहयोग पर निर्भर करते हैं और यह सहयोग नहीं दिया गया तो सरकार का सम्पूर्ण ढाँचा कम से कम सिद्धान्त लड़खड़ा जाएगा। सरकार पर दबाव डालने का यह प्रभावशाली ढंग है। यही कारण था कि असहयोग का कार्यक्रम और गाँधी जी की असाधारण प्रतिभा ने देशवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनमें आशा

.jpg)


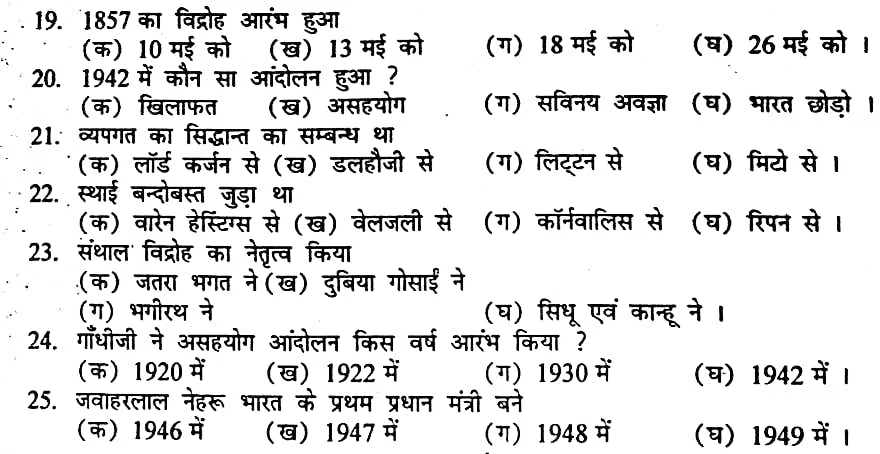


कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें